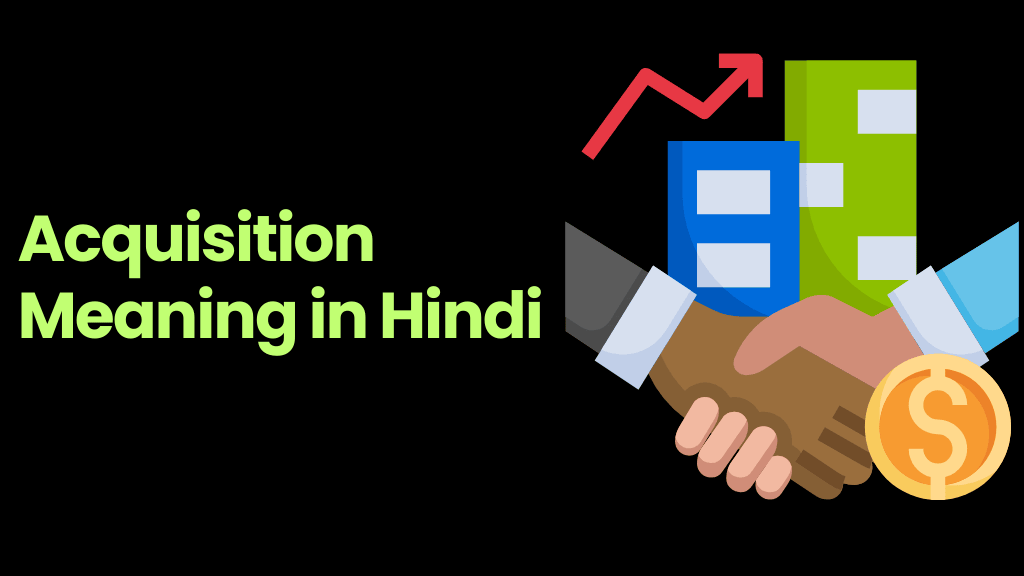जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी, व्यवसाय, संपत्ति या संसाधन को खरीदता है और उसका मालिक बन जाता है, तो उसे Acquisition यानी अधिग्रहण कहा जाता है। हिंदी में Acquisition का मतलब होता है – “किसी वस्तु, संपत्ति या संस्था का अधिग्रहण या स्वामित्व प्राप्त करना।”
इस प्रक्रिया में एक कंपनी दूसरी कंपनी की majority shares (अधिकांश हिस्सेदारी) खरीदकर उसे कंट्रोल कर लेती है। ये अधिग्रहण मित्रतापूर्वक (Friendly Acquisition) भी हो सकता है और कभी-कभी विरोध के साथ (Hostile Acquisition) भी किया जाता है।
Acquisition को आमतौर पर Corporate Strategy का हिस्सा माना जाता है, जिससे कंपनियां अपने business को grow करने, market share बढ़ाने, या किसी new technology या talent को अपनी कंपनी में लाने के लिए इस्तेमाल करती हैं।
आसान भाषा में समझें:
मान लीजिए दो कंपनियां हैं – A और B. अगर कंपनी A, कंपनी B के 51 प्रतिशत या उससे अधिक shares खरीद लेती है, तो अब कंपनी A ही कंपनी B की मालिक बन जाती है। इसे ही हम अधिग्रहण कहते हैं।
What is Acquisition in Hindi – अधिग्रहण क्या है?
अधिग्रहण एक बिजनेस प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को पूरी तरह से या आंशिक रूप से खरीद लेती है। इसका उद्देश्य होता है व्यापार का विस्तार करना, नई टेक्नोलॉजी या संसाधनों तक पहुंच बनाना, या प्रतिस्पर्धा को कम करना।
यह प्रक्रिया तब होती है जब खरीदार कंपनी (Acquiring Company) टारगेट कंपनी (Target Company) के शेयर या सम्पत्ति खरीद लेती है और उसके प्रबंधन और संचालन पर नियंत्रण पा लेती है।
कुछ मुख्य बातें जो Acquisition को समझने में मदद करेंगी:
- यह एक रणनीतिक निर्णय होता है जो मार्केट पोजिशन को मजबूत बनाने में मदद करता है।
- यह केवल बड़ी कंपनियों में ही नहीं, छोटी और मध्यम कंपनियों में भी होता है।
- अधिग्रहण का उपयोग कंपनियां fast growth, geographical expansion या नये प्रोडक्ट लाइन तक पहुंच बनाने के लिए करती हैं।
उदाहरण से समझें:
अगर एक बड़ी कंपनी जैसे Reliance किसी छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी को खरीद लेती है ताकि वह उस कंपनी की तकनीक को अपने सिस्टम में उपयोग कर सके, तो यह अधिग्रहण कहलाएगा।
यह एक सामान्य और जरूरी रणनीति बन चुकी है जिससे कंपनियां तेजी से business को grow करती हैं और नया customer base तैयार करती हैं।
अधिग्रहण का उदाहरण (Example of Acquisition in Hindi)
अधिग्रहण को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ practical उदाहरणों पर नजर डालते हैं। ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि कैसे बड़ी कंपनियां अधिग्रहण के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं और नई संभावनाओं को अपनाती हैं।
उदाहरण 1: Facebook द्वारा WhatsApp का अधिग्रहण
2014 में Facebook ने WhatsApp को लगभग 19 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। यह अधिग्रहण इसलिए किया गया क्योंकि WhatsApp के पास बहुत बड़ा यूजर बेस था, और Facebook उसे अपने प्लेटफॉर्म से जोड़कर सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता था।
उदाहरण 2: Tata Group द्वारा Air India का अधिग्रहण
2022 में Tata Group ने सरकारी विमानन कंपनी Air India का अधिग्रहण किया। यह एक रणनीतिक निर्णय था जिससे टाटा समूह ने aviation सेक्टर में अपनी मजबूत वापसी की। यह अधिग्रहण टाटा समूह के ब्रांड और ट्रस्ट को airline सेक्टर में फिर से स्थापित करने का मौका था।
उदाहरण 3: Zomato द्वारा Blinkit का अधिग्रहण
Zomato ने instant delivery startup Blinkit को अधिग्रहित किया ताकि वह अपने food delivery बिजनेस के साथ grocery और daily essentials की delivery भी कर सके।
इन उदाहरणों से यह समझ में आता है कि Acquisition कंपनियों के लिए growth और diversification का एक जरिया बन चुका है।
अधिग्रहण के प्रकार (Types of Acquisition in Hindi)
अधिग्रहण यानी acquisition कई तरह से किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस उद्देश्य से अधिग्रहण किया जा रहा है और कौन-सी कंपनियां इसमें शामिल हैं। नीचे अधिग्रहण के मुख्य प्रकार दिए गए हैं:
1. Horizontal Acquisition (क्षैतिज अधिग्रहण)
जब कोई कंपनी उसी क्षेत्र या इंडस्ट्री में किसी अन्य प्रतियोगी कंपनी का अधिग्रहण करती है, तो इसे क्षैतिज अधिग्रहण कहा जाता है। इसका उद्देश्य market share बढ़ाना और competition को कम करना होता है।
उदाहरण: Ola द्वारा TaxiForSure का अधिग्रहण।
2. Vertical Acquisition (ऊर्ध्वाधर अधिग्रहण)
इस प्रकार का अधिग्रहण तब होता है जब कोई कंपनी अपने सप्लाई चैन से जुड़ी कंपनी का अधिग्रहण करती है। इससे production से लेकर delivery तक की पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
उदाहरण: एक mobile company द्वारा chipset manufacturer का अधिग्रहण।
3. Conglomerate Acquisition (समूह अधिग्रहण)
जब दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां आपस में जुड़ती हैं, तो इसे समूह अधिग्रहण कहते हैं। इसका उद्देश्य बिजनेस डाइवर्सिफाई करना होता है।
उदाहरण: एक FMCG कंपनी द्वारा एक telecom कंपनी का अधिग्रहण।
4. Friendly Acquisition (मित्रवत अधिग्रहण)
यह अधिग्रहण उस स्थिति में होता है जब target कंपनी सहमति के साथ खुद को बेचती है। दोनों पक्षों में समझौते से सौदा तय होता है।
उदाहरण: Zomato और Uber Eats के बीच का अधिग्रहण।
5. Hostile Acquisition (विरोधी अधिग्रहण)
जब अधिग्रहण बिना लक्ष्य कंपनी की सहमति के किया जाता है, तो उसे hostile acquisition कहा जाता है। यह आमतौर पर शेयर मार्केट के जरिए होता है।
Cost of Acquisition Meaning in Hindi
Cost of Acquisition का मतलब होता है – किसी भी संपत्ति (asset), शेयर, व्यवसाय या कंपनी को हासिल करने में आने वाला कुल खर्च। यह खर्च सिर्फ उस चीज की खरीद मूल्य (purchase price) तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ अन्य जरूरी खर्च भी शामिल होते हैं।
Cost of Acquisition में क्या-क्या शामिल होता है?
- खरीदी गई चीज की actual कीमत
- स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस
- ब्रोकर या एजेंट को दिया गया कमीशन
- कंसल्टेंसी फीस या लीगल खर्च
- ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी खर्च
- अगर renovation की जरूरत पड़ी तो उसका खर्च भी जोड़ा जा सकता है
Tax के नजरिए से Cost of Acquisition क्यों जरूरी है?
Income Tax Act के अनुसार जब आप किसी asset को बेचते हैं तो उसपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन निकालते समय cost of acquisition को घटाया जाता है।
इसलिए, सही cost of acquisition जानना जरूरी है ताकि टैक्स की सही गणना हो सके।
एक Example से समझें:
मान लीजिए आपने एक जमीन ₹10 लाख में खरीदी।
- रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी: ₹50,000
- एजेंट कमीशन: ₹25,000
- लीगल फीस: ₹10,000
तो आपकी total cost of acquisition होगी ₹10,85,000।
जब आप ये जमीन बेचेंगे, तब इसी amount को cost माना जाएगा।
Land Acquisition Meaning in Hindi
Land Acquisition का अर्थ होता है – जब सरकार या कोई अधिकृत संस्था किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की जमीन को किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करती है, तो उसे भूमि अधिग्रहण कहा जाता है।
सरकार यह जमीन सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, डैम, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए लेती है।
भूमि अधिग्रहण कैसे होता है?
भारत में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मुख्य रूप से Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के तहत की जाती है। इस कानून का उद्देश्य है:
- उचित मुआवज़ा देना
- प्रभावित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना
- पारदर्शिता बनाए रखना
Land Acquisition के स्टेप्स:
- ज़रूरत का मूल्यांकन – सरकार यह तय करती है कि जमीन की आवश्यकता है या नहीं
- सूचना जारी करना – अधिसूचना के माध्यम से जमीन मालिकों को सूचित किया जाता है
- मुआवज़ा तय करना – मार्केट वैल्यू और अन्य फैक्टर्स के आधार पर compensation तय होता है
- आपत्ति और सुनवाई – मालिक अगर चाहें तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं
- भूमि अधिग्रहण और भुगतान – अंतिम आदेश के बाद भूमि सरकार के नाम ट्रांसफर हो जाती है और मुआवज़ा दिया जाता है
Land Acquisition उदाहरण:
अगर सरकार किसी गांव में नेशनल हाईवे बनाने की योजना बनाती है और रास्ते में आने वाली जमीन को अधिग्रहित करती है, तो वह land acquisition कहलाएगा। इसके बदले में मालिकों को compensation मिलता है।
Knowledge Acquisition Meaning in Hindi
Knowledge Acquisition का मतलब होता है – ज्ञान या जानकारी को प्राप्त करना, समझना और उसे अपने जीवन या काम में उपयोग करना।
यह एक Learning Process है जिसमें हम नई चीजें सीखते हैं, अनुभवों से ज्ञान पाते हैं और समय के साथ उसे समझने और याद रखने की क्षमता विकसित करते हैं।
Knowledge Acquisition कब और कैसे होता है?
Knowledge Acquisition जीवन के हर क्षेत्र में होता है – चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, या व्यक्तिगत अनुभव। इसे तीन मुख्य तरीकों से समझा जा सकता है:
- Formal Knowledge – जैसे किताबों, स्कूल, कॉलेज या कोर्सेज से मिलने वाला ज्ञान
- Informal Knowledge – जैसे बातचीत, पर्यवेक्षण (Observation), जीवन के अनुभवों से मिलने वाला ज्ञान
- Tacit Knowledge – जो इंसान खुद के अनुभव से सीखता है और दूसरों को समझाना थोड़ा कठिन होता है, जैसे साइकिल चलाना या कोई कला
Knowledge Acquisition का उपयोग कहां होता है?
- Education में – छात्रों को विषयों की जानकारी देने में
- Business में – ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए
- AI और मशीन लर्निंग में – जब मशीनें इंसानों की तरह डेटा से सीखती हैं
- Personal Growth के लिए – ताकि हम जीवन में सही निर्णय ले सकें
Knowledge Acquisition उदाहरण:
अगर कोई बच्चा स्कूल में गणित सीखता है और उसे अपने खर्चों का हिसाब लगाना आता है, तो वह Knowledge Acquisition का एक साधारण उदाहरण है।
Talent Acquisition Meaning in Hindi
Talent Acquisition का मतलब होता है – किसी संगठन (Organization) के लिए सही और योग्य लोगों को पहचानना, आकर्षित करना और उन्हें कंपनी में नियुक्त करना। यह सिर्फ नौकरी भरने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक रणनीतिक तरीका होता है जिससे किसी कंपनी को लंबे समय के लिए अच्छे टैलेंट मिलते हैं।
Talent Acquisition क्या केवल Hiring होती है?
नहीं, टैलेंट एक्विजिशन केवल हायरिंग तक सीमित नहीं होता। इसमें ये सभी स्टेप्स शामिल होते हैं:
- Talent Planning – कंपनी को किस प्रकार के लोग चाहिए, इसका प्लान बनाना
- Attracting Candidates – योग्य लोगों को कंपनी की ओर आकर्षित करना
- Screening और Interviewing – सही कैंडिडेट को पहचानने की प्रक्रिया
- Selecting the Best Fit – सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना
- Onboarding – नए कर्मचारी को कंपनी में अच्छे से शामिल करना
Talent Acquisition की जरूरत क्यों होती है?
- कंपनी के विकास और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए
- भविष्य की जरूरतों के अनुसार स्टाफ तैयार करने के लिए
- एक मजबूत और कुशल टीम बनाने के लिए
Talent Acquisition और Recruitment में क्या अंतर है?
| Talent Acquisition | Recruitment |
|---|---|
| रणनीतिक प्रक्रिया (Strategic Process) | तात्कालिक Hiring Process |
| भविष्य के टैलेंट पर फोकस | वर्तमान की जरूरतें पूरी करना |
| ब्रांडिंग और नेटवर्किंग भी शामिल | सीधा जॉब पोस्ट और चयन |
| लंबा समय लग सकता है | अपेक्षाकृत जल्दी पूरा होता है |
Talent Acquisition उदाहरण:
अगर एक आईटी कंपनी अगले साल एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है और अभी से उसके लिए Data Scientists को ट्रेन कर रही है या हायर कर रही है, तो यह Talent Acquisition का उदाहरण है।
Acquisition के फायदे (Advantages of Acquisition in Hindi)
Acquisition के कई फायदे होते हैं जो किसी कंपनी या संगठन के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नीचे हम कुछ प्रमुख फायदे विस्तार से समझेंगे:
1. बाजार में स्थिति मजबूत होती है (Strengthens Market Position)
जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अधिग्रहित करती है, तो उसे अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले एक मजबूत स्थिति मिलती है। इससे बाजार हिस्सेदारी (Market Share) बढ़ती है और कंपनी का प्रभाव अधिक होता है।
2. नई प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता का लाभ (Access to New Technologies and Expertise)
अधिग्रहण के माध्यम से कंपनी नई तकनीकों और विशेषज्ञता को हासिल कर सकती है। अगर अधिग्रहण की गई कंपनी के पास कुछ विशेष तकनीकी या उत्पाद की जानकारी है, तो उस विशेषज्ञता का फायदा उठाया जा सकता है।
3. वृद्धि और विस्तार (Growth and Expansion)
Acquisition के द्वारा एक कंपनी आसानी से नए बाजारों में प्रवेश कर सकती है। इससे न केवल उसकी भौतिक उपस्थिति बढ़ती है, बल्कि विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का भी विस्तार होता है। इससे कंपनी को नए अवसर और राजस्व का स्रोत मिल सकता है।
4. खर्चों में कमी (Cost Reduction)
कई बार, कंपनियां अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करके अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और लागत में कमी ला सकती हैं। जैसे कि जब दो कंपनियां मिलती हैं, तो वे अपनी संचालन लागत को साझा कर सकती हैं, जिससे दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद स्थिति बनती है।
5. विपणन रणनीतियों में सुधार (Improvement in Marketing Strategies)
अधिग्रहण के बाद कंपनी को नए विपणन (Marketing) साधन और रणनीतियाँ मिल सकती हैं। यह उसे अपने ब्रांड को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद कर सकता है।
Acquisition के नुकसान (Disadvantages of Acquisition in Hindi)
जहां Acquisition के फायदे होते हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जो कंपनी के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। आइए इन नुकसानों को समझें:
1. संस्कृति का टकराव (Cultural Clash)
अधिग्रहण के दौरान, दो कंपनियों की कार्यशैली (Culture) और टीमों का मिलन बहुत कठिन हो सकता है। यदि दोनों कंपनियों की कार्यशैली अलग है, तो कर्मचारियों के बीच असहमति और असुविधा हो सकती है। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है और उत्पादकता पर भी असर पड़ सकता है।
2. मूल्यांकन में गलतियाँ (Mistakes in Valuation)
कभी-कभी कंपनियां दूसरी कंपनियों को अधिग्रहित करते समय गलत मूल्यांकन कर सकती हैं। यह तब होता है जब अधिग्रहण की गई कंपनी का मूल्य अधिक या कम आंका जाता है, जिससे निवेशक को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
3. ऋण का बोझ (Debt Burden)
अधिग्रहण के दौरान, अगर कंपनी दूसरे को खरीदने के लिए कर्ज़ (Debt) लेती है, तो यह कर्ज़ उसे चुकाना पड़ता है। इससे वित्तीय दबाव बढ़ सकता है और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी प्रभावित हो सकती है।
4. नौकरी के अवसर कम होना (Job Loss)
कभी-कभी अधिग्रहण के कारण कर्मचारियों को निकालना पड़ता है, क्योंकि दोनों कंपनियों के समान विभागों के लिए एक ही कर्मचारी का काम हो सकता है। इस प्रकार, कर्मचारियों के लिए नौकरियों का संकट उत्पन्न हो सकता है।
5. ब्रांड की छवि पर असर (Impact on Brand Image)
अधिग्रहण के बाद, अगर सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता, तो कंपनी की ब्रांड छवि प्रभावित हो सकती है। पुराने ग्राहक जो एक विशेष कंपनी से जुड़े थे, वे नए स्वामित्व के साथ जुड़ने में असहज महसूस कर सकते हैं।
Acquisition Meaning in Hindi: इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातें
इस अध्याय में, हम Acquisition (अधिग्रहण) के महत्व को संक्षेप में समझेंगे और इस पर आधारित कुछ प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। अधिग्रहण का अर्थ, इसके प्रकार, प्रक्रिया, फायदे और नुकसान को समझने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी व्यवसाय या संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
अधिग्रहण की प्रक्रिया, सही तरीके से किए गए मूल्यांकन, और सही रणनीति से यह किसी भी संगठन के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया के दौरान संभावित जोखिमों को समझा जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके।
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए:
- अधिग्रहण के प्रकार को समझना – अधिग्रहण के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे कि Horizontal Acquisition, Vertical Acquisition, और Conglomerate Acquisition। हर प्रकार की अधिग्रहण प्रक्रिया के अलग-अलग उद्देश्य और फायदे होते हैं।
- सही मूल्यांकन का महत्व – जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अधिग्रहित करती है, तो सही मूल्यांकन (Valuation) करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई वित्तीय नुकसान न हो और कंपनी को सही मूल्य पर अधिग्रहण मिले।
- कर्मचारियों और संस्कृति का एकीकरण – किसी भी अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों और कंपनी की संस्कृति का एकीकरण महत्वपूर्ण होता है। अगर दोनों कंपनियों की कार्यशैली अलग है, तो यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- अधिग्रहण से संबंधित कानूनी प्रक्रिया – अधिग्रहण के दौरान, कानूनी प्रक्रिया को समझना और इसे सही तरीके से लागू करना बहुत जरूरी होता है। इससे बाद में कानूनी परेशानियाँ नहीं होतीं।
अधिग्रहण के लिए उचित योजनाओं और रणनीतियों की आवश्यकता होती है ताकि यह पूरी प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न हो सके।

Pradeep, with over 5 years of experience in the stock market, shares valuable insights, tips, and strategies on ShareMarketPDF.in. Through his expertise, he simplifies complex market concepts, answers readers’ queries, and provides helpful PDFs to support your learning journey. Whether you’re a beginner or an active trader, Pradeep’s practical knowledge can help you navigate the stock market with confidence.